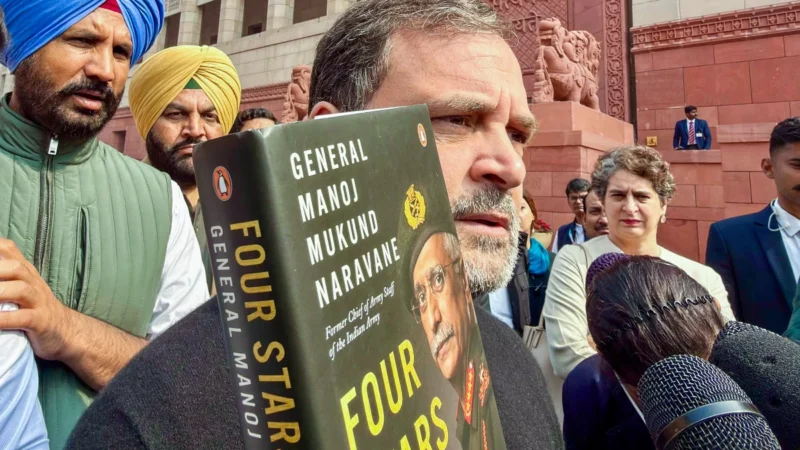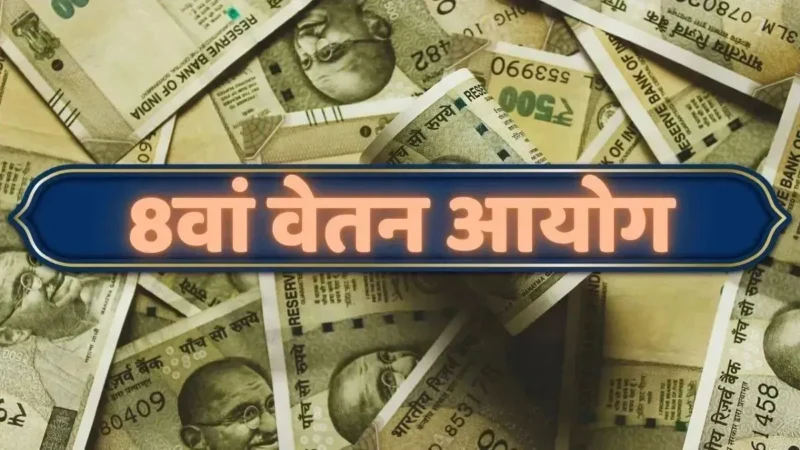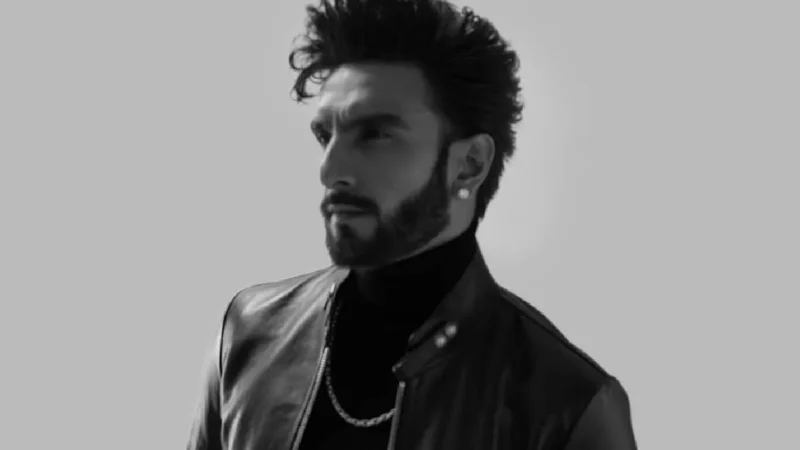सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर की सख्त टिप्पणी- ”क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना सांप्रदायिकता जितना खतरनाक है”

हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना शिवसेना के अध्यक्ष तिरुपति नरसिंह मुरारी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा वोट पाने के लिए क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत की एकता और अखंडता के लिए उतना ही खतरनाक है, जितना समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा, “क्षेत्रीय दल खुलेआम क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं और चुनावों के दौरान इसी आधार पर वोट मांगते हैं। क्या यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं है?” यह टिप्पणी उस वक्त आई जब अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का पंजीकरण रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब कई राजनीतिक दल सांप्रदायिकता में लिप्त हैं, तब वह किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बना सकती।
हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना शिवसेना के अध्यक्ष तिरुपति नरसिंह मुरारी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां कीं हैं, वे केवल इस मामले तक सीमित नहीं हैं बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था की गहराई से पड़ताल करने का अवसर भी देती हैं।
हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का तर्क था कि AIMIM का संविधान और उसकी गतिविधियां भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ हैं। उनका कहना था कि AIMIM केवल मुस्लिम समुदाय के हित में काम कर रही है, जो संविधान के मूल स्वरूप के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि AIMIM धार्मिक ग्रंथों का प्रचार-प्रसार करती है, जो राजनीतिक दलों के लिए अनुचित है। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी याचिकाएं केवल किसी एक पार्टी या व्यक्ति को लक्षित करके नहीं लानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि “आप ऐसी याचिका दाखिल करें जो किसी एक दल तक सीमित न हो। केवल सांप्रदायिकता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। क्षेत्रीय दल भी जाति आधारित राजनीति करते हैं और यह भी उतना ही खतरनाक है।” अदालत ने कहा कि समस्या व्यापक है। सुधार राजनीतिक दलों के सिद्धांतों और आचरण में होने चाहिए। अपनी टिप्पणी में न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कीं- 1. धर्म या जाति के नाम पर राजनीति केवल एक पार्टी की समस्या नहीं है, यह पूरे तंत्र की कमजोरी है। 2. राजनीतिक सुधार की मांग व्यापक होनी चाहिए, न कि किसी विशेष पार्टी के विरोध में।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह स्वीकार किया कि भारत में कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल धर्म, जाति, समुदाय आधारित राजनीति को बढ़ावा देते हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को भीतर से खोखला करती है और मतदाताओं को सामाजिक आधार पर विभाजित करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक कोई पार्टी खुलकर संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रही, तब तक उसकी मान्यता समाप्त करने का कोई आधार नहीं बनता। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि वे वास्तव में सुधार चाहते हैं, तो ऐसी याचिका दाखिल करें जो सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान हो और तंत्र के भीतर व्यापक सुधार की मांग करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा की गई है और किसी भी धर्म के कमजोर वर्गों के हित में काम करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। साथ ही, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या शिक्षण भी कोई अपराध नहीं है और इसे आपत्तिजनक नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर गौर करें तो जो बातें स्पष्ट होती हैं वह यह हैं कि न्यायपालिका राजनीतिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप से बच रही है, विशेषकर जब याचिका किसी एक विशेष पार्टी या व्यक्ति को निशाना बनाकर दाखिल की गयी हो। साथ ही संपूर्ण राजनीतिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता को सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकार कर रहा है। इस मामले में अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि देश के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल अक्सर जाति और धर्म आधारित राजनीति करते हैं और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। परंतु किसी एक दल को अलग से अपराधी घोषित करना समाधान नहीं है, बल्कि राजनीतिक सुधारों के लिए व्यापक नीतिगत और कानूनी बहस की आवश्यकता है।
देखा जाये तो न्यायपालिका का यह रुख संकेत करता है कि भविष्य में ऐसी याचिकाएं दाखिल हों जो सभी दलों की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग करें, न कि केवल सांप्रदायिकता या धर्म के नाम पर किसी एक पार्टी को निशाना बनाकर याचिकाएं दाखिल की जाएं। भारत में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका इस संदर्भ में और मजबूत करने की जरूरत है ताकि वे यह तय कर सकें कि कोई भी पार्टी संविधान के मूल्यों के विरुद्ध कार्य न करे। इस पूरे मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत की न्यायपालिका अब उन याचिकाओं को तरजीह नहीं देगी जो राजनीति में केवल एकपक्षीय या पूर्वाग्रही दृष्टिकोण से दाखिल की जाएं। आने वाले समय में अगर राजनीति में सुधार की बात होती है, तो यह सिर्फ धर्म या जाति आधारित पार्टियों पर नहीं, बल्कि हर उस दल पर लागू होगी जो किसी भी प्रकार की वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है।
बहरहाल, AIMIM के पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को केवल एक अदालती निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करने वाली टिप्पणी है। उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ कहा है उससे उम्मीद है कि देश में धर्म, जाति, समुदाय आधारित राजनीति करने वाले दलों और नेताओं के विरुद्ध जनमत तैयार होगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख बताता है कि भारत को अब ऐसी नीतिगत बहस और कानून की जरूरत है जो सभी दलों को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और पारदर्शी मूल्यों के तहत चलने के लिए बाध्य करे।